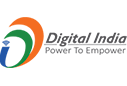पूछे जाने वाले प्रश्न
1. मध्यस्थता क्या है?
मध्यस्थता एक बातचीत की प्रक्रिया है जिसमें एक तटस्थ तीसरा पक्ष विवाद करने वाले पक्षों को उनके विवाद को सुलझाने में सहायता करता है। मध्यस्थ पक्षों को समझौता करने में मदद करने के लिए विशेष बातचीत और संचार तकनीकों का उपयोग करता है। पक्ष अपनी आपसी सहमति से मध्यस्थ नियुक्त कर सकते हैं (या) किसी लंबित मुकदमे में न्यायालय द्वारा मध्यस्थ नियुक्त किया जा सकता है। मध्यस्थता हमेशा निर्णय लेने की शक्ति पक्षों के पास छोड़ती है। मध्यस्थ यह तय नहीं करता कि क्या उचित या सही है, दोष नहीं बांटता, न ही मुकदमेबाजी होने पर सफलता की संभावनाओं या योग्यता पर कोई राय देता है। इसके बजाय, मध्यस्थ मुद्दों को परिभाषित करके और संचार और समझौते में बाधाओं को सीमित करके दो विवादित पक्षों को एक साथ लाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
2. धारा 89 सीपीसी के तहत एडीआर प्रक्रियाएं क्या हैं?
धारा 89 पांच प्रकार की ए.डी.आर. प्रक्रियाओं का उल्लेख करती है, जिनमें एक है; न्यायिक प्रक्रिया (मध्यस्थता) और चार वार्तात्मक प्रक्रियाएं (गैर न्यायिक) अर्थात समझौता, मध्यस्थता, न्यायिक समझौता और लोक अदालत।
सी.पी.सी. की धारा 89 यह स्पष्ट करती है कि ए.डी.आर. प्रक्रियाओं में से दो अर्थात मध्यस्थता और समझौता मध्यस्थता और समझौता अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होंगी तथा दो अन्य ए.डी.आर. प्रक्रियाएं अर्थात लोक अदालत समझौता और मध्यस्थता विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम द्वारा शासित होंगी। (एफकॉन के इन्फ्रा जजमेंट में न्यायिक व्याख्या द्वारा संशोधित सी.पी.सी. की धारा 89 (2) (सी) देखें)
3. मध्यस्थता के प्रकार क्या हैं?
मध्यस्थता के दो प्रकार हैं:
- न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट मध्यस्थता- यह न्यायालय में लंबित मामलों पर लागू होता है और जिन्हें न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 के अंतर्गत मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा।
- निजी मध्यस्थता – निजी मध्यस्थता में, योग्य मध्यस्थ न्यायालय, जनता, वाणिज्यिक क्षेत्र के सदस्यों और सरकारी क्षेत्र को मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को हल करने के लिए निजी, शुल्क-सेवा के आधार पर अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं। निजी मध्यस्थता का उपयोग न्यायालय में लंबित विवादों और मुकदमे-पूर्व विवादों के संबंध में किया जा सकता है।
4. मध्यस्थ की योग्यताएं क्या हैं?
निम्नलिखित व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के पात्र हैं:
-
-
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश
- उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश
- सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश या समकक्ष स्थिति वाले न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश
- उच्चतर न्यायिक सेवाओं के न्यायिक अधिकारी
-
- सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या समकक्ष स्तर पर वकालत करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले कानूनी व्यवसायी।
- कम से कम पंद्रह वर्षों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य पेशेवर; या सेवानिवृत्त वरिष्ठ नौकरशाह या सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी।
5. मध्यस्थ के कार्य क्या हैं?
मध्यस्थ के कार्य निम्नलिखित हैं:
- मध्यस्थता की प्रक्रिया को सुगम बनाना; और
- किसी समझौते पर पहुंचने के लिए मामले का मूल्यांकन करने में पक्षों की सहायता करना।
6. प्रशिक्षित मध्यस्थ कौन है?
प्रशिक्षित मध्यस्थ वह होता है जिसने मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति, नई दिल्ली द्वारा 40 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तथा न्यायालय को लंबित मामलों को केवल प्रशिक्षित मध्यस्थ को ही भेजना चाहिए।
7. क्या प्रत्येक जिले में प्रशिक्षित मध्यस्थ उपलब्ध हैं?
हाँ। हमारे पास हर जिले में एमसीपीसी (40) घंटे प्रशिक्षित मध्यस्थ हैं।
8. क्या न्यायाधीशों को मध्यस्थ के रूप में भी प्रशिक्षित किया जाता है?
हाँ। हमारे राज्य में न्यायाधीश-प्रशिक्षित मध्यस्थ भी उपलब्ध हैं। पक्षकार मध्यस्थता केंद्र के समन्वयक से एक न्यायाधीश-प्रशिक्षित मध्यस्थ नियुक्त करने का अनुरोध भी कर सकते हैं, जो उनकी उपलब्धता के आधार पर उनके अनुरोध पर विचार करेगा।
9. लंबित विवाद को किस स्तर पर धारा 89 सीपीसी के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है?
जब अभिवचन पूरे हो जाएं, तो मुद्दे तय करने से पहले, न्यायालय पक्षकारों की उपस्थिति के लिए प्रारंभिक सुनवाई तय करेगा और न्यायालय को मामले के तथ्यों और पक्षकारों के बीच विवाद की प्रकृति से परिचित होना चाहिए और जिन मामलों को एडीआर प्रक्रियाओं के लिए भेजा जा सकता है, न्यायालय को पक्षकारों को एडीआर प्रक्रियाओं के विकल्प के बारे में समझाना चाहिए ताकि वे अपने विकल्प का प्रयोग कर सकें, यदि पक्षकार मध्यस्थता और सुलह के लिए सहमत नहीं हैं, तो न्यायालय उन मामलों में मध्यस्थता के लिए मामला भेज सकता है जहां जटिल प्रश्न शामिल हैं या मामलों में कई दौर की बातचीत की आवश्यकता है।
10. क्या पारिवारिक और वैवाहिक विवादों को भी दलीलें पूरी होने के बाद संदर्भित किया जा सकता है?
नहीं। पारिवारिक विवादों या वैवाहिक मामलों में, स्थिति थोड़ी अलग होती है। इन मामलों में, पति/पत्नी के विरुद्ध याचिका में लगाए गए विभिन्न आरोपों के कारण रिश्ते में दुश्मनी हो जाती है और प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित बयान या प्रतिवाद में लगाए गए प्रति-आरोपों से यह दुश्मनी और भी बढ़ जाती है। इसलिए, जहाँ तक पारिवारिक विवादों का संबंध है, मध्यस्थता के लिए आदर्श चरण प्रतिवादी के उपस्थित होने के तुरंत बाद और प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद/लिखित बयान दाखिल करने से पहले होगा।
11. जब कोई मामला धारा 89 सीपीसी के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है तो प्रक्रिया क्या है?
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि मध्यस्थता के लिए संदर्भ केवल तभी हो सकता है जब पक्षों के बीच पहले से मौजूद मध्यस्थता समझौता हो। यदि पक्षों के बीच पहले से मौजूद मध्यस्थता समझौता होता, तो सभी संभावनाओं में, मुकदमे के ऑर्डर एक्स सीपीसी के चरण तक पहुंचने से पहले ही मामला धारा 89 सीपीसी का सहारा लिए बिना मध्यस्थता के लिए भेजा गया होता। यहां तक कि अगर कोई पहले से मौजूद मध्यस्थता समझौता नहीं है, तो मुकदमे के पक्ष मध्यस्थता के लिए सहमत हो सकते हैं जब अदालत द्वारा धारा 89 सीपीसी के तहत एडीआर प्रक्रियाओं का विकल्प उन्हें पेश किया जाता है। इस तरह का समझौता संयुक्त ज्ञापन (या) संयुक्त आवेदन (या) न्यायालय के समक्ष एक संयुक्त हलफनामे के माध्यम से (या) पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित आदेश पत्र में अदालत द्वारा समझौते के रिकॉर्ड द्वारा किया जा सकता है।
12. क्या सहमति के अभाव में मामले को धारा 89 सीपीसी के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है?
<p class=”text-justify”>नहीं। यदि पक्षकारों के बीच मध्यस्थता के लिए सहमति नहीं है, तो न्यायालय मामले को धारा 89 सीपीसी के अंतर्गत मध्यस्थता के लिए नहीं भेज सकता। धारा 89 सीपीसी के अंतर्गत मध्यस्थता के लिए संदर्भ केवल दोनों पक्षों की सहमति से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। एक बार मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के बाद, मामला स्थायी रूप से न्यायालय की धारा से बाहर चला जाएगा और वापस न्यायालय में नहीं आएगा।</p>
13. धारा 89 सीपीसी के तहत लंबित मामले को संदर्भित करने की प्रक्रिया क्या है?
यदि संदर्भ मध्यस्थता या सुलह का है, तो न्यायालय को यह दर्ज करना होगा कि संदर्भ आपसी सहमति से है। आदेश पत्र में इसके अलावा कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं है।
यदि संदर्भ किसी अन्य एडीआर प्रक्रिया का है, तो न्यायालय को संक्षेप में यह दर्ज करना चाहिए कि विवाद की प्रकृति को देखते हुए, मामला लोक अदालत, मध्यस्थता या न्यायिक समाधान, जैसा भी मामला हो, के लिए भेजा जाना चाहिए। संदर्भ देने के लिए विस्तृत आदेश की आवश्यकता नहीं है।
14. क्या एडीआर प्रक्रिया द्वारा निपटान स्वयं में बाध्यकारी है?
जब अदालत सीपीसी की धारा 89 के तहत मध्यस्थता के लिए भेजती है, तो मामला अदालत की धारा से बाहर निकलकर मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष एक स्वतंत्र कार्यवाही बन जाता है। मध्यस्थता एक न्यायिक प्रक्रिया होने के कारण, यह हमेशा एक निर्णय पर समाप्त होती है और मध्यस्थता न्यायाधिकरण प्रक्रिया के विफल होने या मामले को विफलता रिपोर्ट के साथ अदालत में वापस भेजे जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मध्यस्थ का निर्णय पक्षों पर बाध्यकारी होता है और न्यायालय के आदेश की तरह निष्पादन योग्य होता है।
जब कोई मामला सुलह के माध्यम से निपटाया जाता है, तो समझौता मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 74 के साथ पठित 30 के तहत न्यायालय के आदेश के समान लागू होता है।
इसी प्रकार, जब लोक अदालत के समक्ष समझौता होता है, तो पंचाट को सिविल न्यायालय का आदेश माना जाता है तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 21 के अनुसार निष्पादन योग्य माना जाता है।
जहां मामला निपटान के लिए किसी अन्य न्यायाधीश को भेजा जाता है और उसके समक्ष निपटाया जाता है, वहां ऐसा समझौता उस न्यायालय के समक्ष भी रखा जाएगा जिसने मामला भेजा था और न्यायालय उसके अनुसार डिक्री जारी करेगा।
जब मामला एफकॉन के इन्फ्रा जजमेंट द्वारा संशोधित सीपीसी की धारा 89(2)(सी) के तहत मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जाता है, तो समझौते की शर्तों को लिखित रूप में कम कर दिया जाएगा और इसे रेफरल जज के समक्ष रखा जाएगा और रेफरल जज समझौते की शर्तों की वैधता और प्रवर्तनीयता के अधीन जांच करेगा और एक डिक्री पारित करेगा और उक्त डिक्री पक्षों पर बाध्यकारी है क्योंकि इसे लोक अदालत के पुरस्कार का दर्जा प्राप्त है।
15. मध्यस्थता में रेफरल न्यायाधीशों की भूमिका क्या है?
वे न्यायाधीश जो सीपीसी की धारा 89 के अंतर्गत किसी भी एडीआर विधि के माध्यम से मामलों को निपटान के लिए भेजते हैं, उन्हें रेफरल न्यायाधीश कहा जाता है। सभी मामले मध्यस्थता के लिए उपयुक्त हैं। मध्यस्थता की सफलता मुख्यतः रेफरल न्यायाधीशों द्वारा उचित चयन और केवल उपयुक्त मामलों के संदर्भ पर निर्भर करेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एफकॉन निर्णय के आलोक में, एक रेफरल न्यायाधीश को संदर्भ की शर्तें तैयार करने या उन्हें पक्षकारों के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। उनसे केवल एडीआर को संदर्भित करने के लिए मामले की उपयुक्तता का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने की अपेक्षा की जाती है।
16. क्या रेफरल जज पक्षों को मध्यस्थता के लिए राजी और प्रेरित कर सकता है?
मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए पक्षों को प्रेरित करने में रेफरल न्यायाधीश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि पक्ष मध्यस्थता के लिए सहमत नहीं हैं, तो रेफरल न्यायाधीश उनकी अनिच्छा का पता लगाकर उन्हें मध्यस्थता के लिए राजी और प्रेरित कर सकते हैं। उन्हें मध्यस्थता के लाभों की अवधारणा और मध्यस्थता के माध्यम से समाधान कैसे पक्षों के अंतर्निहित हितों को संतुष्ट कर सकता है, इसकी व्याख्या करनी चाहिए।
17. मध्यस्थता पूरी होने के बाद रेफरल जज की भूमिका क्या है?
मध्यस्थता के समापन के बाद भी रेफरल न्यायाधीश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मामले पर उनका नियंत्रण और अधिकार क्षेत्र बना रहता है, मध्यस्थता के परिणाम को उचित आदेश पारित करने के लिए न्यायालय के समक्ष रखा जाना चाहिए।
यदि मध्यस्थता के माध्यम से समझौता हो जाता है, तो रेफरल न्यायाधीश को यह जाँच करनी चाहिए कि क्या पक्षों के बीच हुआ समझौता वैध और प्रवर्तनीय है। यदि समझौता की विषयवस्तु प्रवर्तनीय नहीं है, तो उसे पक्षों के ध्यान में लाया जाना चाहिए और रेफरल न्यायाधीशों को ऐसे समझौते पर कार्रवाई करने से बचना चाहिए। यदि समझौता वैध और प्रवर्तनीय पाया जाता है, तो रेफरल न्यायाधीश को समझौते की शर्तों के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए और आदेश पारित करना चाहिए। एफकॉन के इन्फ्रा जजमेंट में धारा 89(2)(सी) के न्यायिक संशोधन के मद्देनजर, ऐसा निर्णय लोक अदालत के अंतिम निर्णय के समान है, और ऐसे समझौते पर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।
यदि पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं होता है, तो अदालती कार्यवाही कानून के अनुसार जारी रहेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मध्यस्थता प्रक्रिया की गोपनीयता का उल्लंघन रेफरल जज द्वारा न हो, उसे पक्षों के बीच समझौता न हो पाने का कारण नहीं पूछना चाहिए। मध्यस्थता प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, रेफरल जज और मध्यस्थ के बीच मध्यस्थता के संबंध में कोई संवाद नहीं होना चाहिए।
18. मामले को संदर्भित करने से पहले निपटान की शर्तों को तैयार करने या पुनः तैयार करने के लिए सीपीसी की धारा 89 (1) की आवश्यकताओं का अनुपालन कैसे करें?
धारा 89(1) सीपीसी की आवश्यकता यह है कि न्यायालय को निपटान की शर्तों को तैयार या पुनः तैयार करना चाहिए, इसका मतलब केवल यह होगा कि न्यायालय को विवाद की प्रकृति का संक्षेप में उल्लेख करना होगा और उचित एडीआर प्रक्रिया (एफकॉन्स जजमेंट) पर निर्णय लेना होगा। यह पर्याप्त है कि न्यायालय विवाद की प्रकृति (एक या दो वाक्यों में) का उल्लेख करता है और संदर्भ देता है।
19. एडीआर प्रक्रिया के लिए सामान्यतः क्या समय सीमा निर्धारित की जाती है?
यदि न्यायालय मामले को मध्यस्थता प्रक्रिया (मध्यस्थता के अलावा) के लिए भेजता है, तो उसे मध्यस्थता रिपोर्ट की सुनवाई की तिथि निर्धारित करके मामले पर नज़र रखनी चाहिए। मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए आवंटित अवधि सामान्यतः एक सप्ताह से दो महीने तक हो सकती है (जिसे वैकल्पिक मंच की उपलब्धता, मामले की प्रकृति आदि के आधार पर असाधारण मामलों में बढ़ाया जा सकता है)। एमसीपीसी नियम, 2015 के नियम 18 के अनुसार, मध्यस्थ के समक्ष पक्षों की पहली उपस्थिति के लिए निर्धारित तिथि से (90) दिन का समय होता है।
20. किस श्रेणी के मामलों को सामान्यतः एडीआर प्रक्रिया के लिए अनुपयुक्त माना जाता है?
-
- सीपीसी के नियम 8 के तहत प्रतिनिधि मुकदमें, जिनमें सार्वजनिक हित या ऐसे अनेक व्यक्तियों का हित शामिल हो जो न्यायालय के समक्ष पक्षकार न हों।
- सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव से संबंधित विवाद।
- जांच के बाद न्यायालय द्वारा प्राधिकार प्रदान करने से संबंधित मामले, उदाहरण के लिए, प्रोबेट या प्रशासन पत्र प्रदान करने के लिए मुकदमे।
- धोखाधड़ी, दस्तावेजों की जालसाजी, जालसाजी, प्रतिरूपण, जबरदस्ती आदि के गंभीर और विशिष्ट आरोपों से जुड़े मामले।
- ऐसे मामले जिनमें न्यायालयों के संरक्षण की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए, नाबालिगों, देवताओं और मानसिक रूप से विकलांगों के विरुद्ध दावे और सरकार के विरुद्ध स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमे।
- आपराधिक अपराधों के लिए अभियोजन से संबंधित मामले।
सिविल प्रकृति के अन्य सभी मामले चाहे वे सिविल न्यायालयों या अन्य विशेष न्यायाधिकरणों में लंबित हों या सामान्यतः ए.डी.आर. प्रक्रिया के लिए उपयुक्त हों।
21. क्या एडीआर प्रक्रिया का संदर्भ अनिवार्य है?
जहां मामला उपर्युक्त बहिष्कृत श्रेणी के अंतर्गत आता है, वहां एडीआर प्रक्रिया का संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अन्य सभी मामलों में एडीआर प्रक्रिया का संदर्भ देना अनिवार्य है।
22. मध्यस्थता की प्रक्रिया और चरणों को संक्षेप में समझाइए?
मध्यस्थता एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें मध्यस्थ पक्षों को विवाद सुलझाने के लिए समझौता वार्ता करने में सहायता करता है। ऐसा करते समय, मध्यस्थ मध्यस्थता के चार कार्यात्मक चरणों का उपयोग करता है, अर्थात्,
- परिचय एवं आरंभिक वक्तव्य।
- संयुक्त सत्र।
- अलग सत्र।
- समापन।
23. मध्यस्थता के क्या लाभ हैं?
मध्यस्थता के लाभ
-
- पक्षों का मध्यस्थता पर नियंत्रण होता है
-
- इसका दायरा; और
- इसका परिणाम (अर्थात, उन्हें यह निर्णय लेने का अधिकार है कि समझौता करना है या नहीं और समझौते की शर्तें क्या होंगी।)
-
- मध्यस्थता सहभागी होती है। पक्षों को अपने शब्दों में अपना मामला प्रस्तुत करने और बातचीत में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अवसर मिलता है।
- यह प्रक्रिया स्वैच्छिक है और कोई भी पक्ष इसे किसी भी स्तर पर छोड़ सकता है यदि उसे लगता है कि इससे उसे कोई मदद नहीं मिल रही है। मध्यस्थ पक्षों की सहमति के बिना किसी भी समझौते के लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकते।
- यह प्रक्रिया त्वरित, कुशल और किफायती है।
- प्रक्रिया सरल और लचीली है। इसे प्रत्येक मामले की आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।
- यह प्रक्रिया अनौपचारिक, सौहार्दपूर्ण और अनुकूल वातावरण में आयोजित की जाती है।
- मध्यस्थता एक निष्पक्ष प्रक्रिया है। मध्यस्थ निष्पक्ष, तटस्थ और स्वतंत्र होता है।
- यह प्रक्रिया गोपनीय है।
- यह प्रक्रिया पक्षों के बीच बेहतर और प्रभावी संचार की सुविधा प्रदान करती है जो रचनात्मक और सार्थक बातचीत के लिए महत्वपूर्ण है।
- मध्यस्थता पक्षों के बीच संबंधों को बनाए रखने/सुधारने/बहाल करने में मदद करती है।
- मध्यस्थता में विवाद समाधान प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में पक्षों के दीर्घकालिक और अंतर्निहित हितों को हमेशा ध्यान में रखा जाता है।
- मध्यस्थता में, विवाद को पारस्परिक रूप से लाभकारी तरीके से सुलझाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- मध्यस्थता से अक्सर पक्षों के बीच संबंधित/जुड़े मामलों का निपटारा हो जाता है।
- मध्यस्थता विवाद समाधान में रचनात्मकता की अनुमति देती है।
- जब पक्षकार स्वयं समझौते की शर्तों पर हस्ताक्षर करते हैं, तथा अपनी अंतर्निहित आवश्यकताओं और हितों को संतुष्ट करते हैं, तो अनुपालन होगा।
- मध्यस्थता अंतिमता को बढ़ावा देती है।
- न्यायालय द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से निपटारे के मामलों में एपीसीएफ एवं एसवी अधिनियम की धारा 66(ए) के अनुसार न्यायालय शुल्क की वापसी की अनुमति है।
- पक्षों का मध्यस्थता पर नियंत्रण होता है
24. मध्यस्थता में वकीलों की क्या भूमिका है?
यद्यपि मध्यस्थता में वकील की भूमिका मुकदमेबाजी में उसकी भूमिका से कार्यात्मक रूप से भिन्न होती है, फिर भी मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान पक्षकार को वकील द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा एक पेशेवर सेवा होती है। मध्यस्थता प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका होती है। उन्हें मध्यस्थता की अवधारणा और प्रक्रिया तथा मध्यस्थता में पक्षकारों की सहायता करने में उनकी सकारात्मक भूमिका का ज्ञान होना चाहिए। वास्तव में, वकील की भूमिका मामले के अदालत में आने से पहले ही शुरू हो जाती है और मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद भी जारी रहती है, चाहे विवाद का निपटारा हुआ हो या नहीं।
25. मध्यस्थता में पक्षों की भूमिका क्या है?
जहाँ तक पक्षकारों का संबंध है, मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया स्वैच्छिक है, विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुँचने में उनकी प्रत्यक्ष, सक्रिय और निर्णायक भूमिका होती है। न तो मध्यस्थ और न ही वकील पक्षकारों के लिए कोई निर्णय लेते हैं। उन्हें पक्षकारों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देनी चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, हालाँकि, पक्षकार मध्यस्थता के संबंध में अपने वकीलों की सेवाएँ लेने के लिए स्वतंत्र हैं।
26. क्या मध्यस्थता के माध्यम से हुए समझौते में पक्षकार न्यायालय शुल्क की वापसी के हकदार हैं?
हाँ। न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, या एपी न्यायालय शुल्क और वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 66 (ए) के अनुसार, जब भी लंबित विवाद को सीपीसी की धारा 89 के तहत निपटान के किसी भी तरीके के लिए संदर्भित किया जाता है, तो वादी न्यायालय से एक प्रमाण पत्र के लिए हकदार है जो कलेक्टर से ऐसे मुकदमे के संबंध में भुगतान की गई न्यायालय शुल्क की पूरी राशि वापस प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है।
27. क्या किसी मध्यस्थ को किसी कार्यवाही में गवाही देने या मध्यस्थता के दौरान क्या हुआ, इसका खुलासा करने के लिए बुलाया जा सकता है?
नहीं। मध्यस्थ को किसी कार्यवाही में गवाही देने या मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ, यह अदालत को बताने के लिए नहीं बुलाया जा सकता।
28. विवाद का निपटारा न हो पाने की स्थिति में मध्यस्थ की रिपोर्ट क्या होगी?
विवाद का निपटारा न होने की स्थिति में, मध्यस्थ विफलता का कारण नहीं बताता। रिपोर्ट में केवल “निपटारा नहीं हुआ” लिखा होगा।
1. निःशुल्क कानूनी सहायता क्या है?
- एक कानूनी व्यवसायी द्वारा कानूनी सलाह।
- किसी भी कानूनी कार्यवाही में हकदार व्यक्ति की ओर से प्रतिनिधित्व करना।
- हकदार व्यक्ति को या उसकी ओर से भुगतान:
-
- न्यायालय शुल्क का,
- प्रक्रिया शुल्क और गवाहों के खर्च,
- कागज़ की किताब तैयार करने के शुल्क, जिसमें दस्तावेजों के मुद्रण और अनुवाद के शुल्क भी शामिल हैं,
- निर्णयों और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति के लिए शुल्क,
- किसी भी कानूनी कार्यवाही में किसी अन्य खाते में किसी भी राशि का।
-
2. निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए कौन पात्र है?
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे कोई मामला दायर करना है या बचाव करना है, अधिनियम के तहत कानूनी सेवाओं का हकदार होगा यदि वह व्यक्ति-
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य (इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर);
- भारतीय संविधान, 1950 के अनुच्छेद 23 में उल्लिखित मानव तस्करी का शिकार या भिखारी;
- महिला या बच्चा;
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित कानूनों में परिभाषित विकलांगता वाला व्यक्ति;
- अपर्याप्त परिस्थितियों में रहने वाला व्यक्ति, जैसे कि किसी सामूहिक आपदा, जातीय, हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा का शिकार होना;
- औद्योगिक कामगार;
- हिरासत में रहने वाला व्यक्ति, जिसमें अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) की धारा 2 के खंड (छ) के अर्थ में संरक्षण गृह में हिरासत में रहना, या किसी संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षा स्थल में रहना शामिल है। किशोर न्याय कानूनों के तहत बाल गृह में, या मानसिक स्वास्थ्य देखभाल कानूनों के तहत किसी मनोरोग अस्पताल या मनोरोग नर्सिंग होम में; या
- यदि मामला सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में है, तो 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति, और यदि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, तो बारह हजार रुपये से कम या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य उच्चतर राशि।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 13 (1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो धारा 12 के तहत किसी भी मानदंड को पूरा करता है, कानूनी सेवाएँ प्राप्त करने का हकदार है, बशर्ते कि संबंधित विधिक सेवा संस्थान इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति के पास मुकदमा चलाने या बचाव करने के लिए एक वास्तविक मामला है। इसलिए, इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार के मामलों के लिए आवेदन कर सकता है और किस प्रकार के मामलों के लिए नहीं। सभी प्रकार के मामले इसमें शामिल हैं, बशर्ते व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत पात्रता पूरी करता हो।
3. क्या आय प्रमाणित करने के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
नहीं। जब कोई व्यक्ति आय के आधार पर मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर रहा है, तो उसके द्वारा अपनी आय के बारे में दिया गया हलफनामा उसे पात्र बनाने के लिए पर्याप्त है, जब तक कि संबंधित प्राधिकारी के पास विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत उल्लिखित हलफनामे पर अविश्वास करने का कारण न हो।
4. क्या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के तहत उल्लिखित जाति को साबित करने के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है?
हां, जाति प्रमाण पत्र की एक प्रति आवश्यक है।
5. क्या आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र है?
हाँ, कोई भी महिला अपनी आय या वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना मुफ़्त कानूनी सहायता पाने की हकदार है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12(सी) के तहत कोई भी महिला मुफ़्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन करने की पात्र है।
6. किस आयु तक कोई बच्चा निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र है?
एक बच्चा वयस्क होने तक यानी 18 वर्ष की आयु तक मुफ़्त कानूनी सहायता पाने का पात्र है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 (सी) में इसका प्रावधान है। इसलिए, कोई भी बच्चा 18 वर्ष की आयु तक मुफ़्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। वयस्क होने पर भी, यदि बच्चा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 में सूचीबद्ध अन्य मानदंडों को पूरा करता है, तो उसे मुफ़्त कानूनी सहायता मिलती रहेगी।
7. क्या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्ति की तरह निःशुल्क कानूनी सहायता का हकदार है?
नहीं। वह केवल तभी हकदार हो सकता है, जब वह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 में उल्लिखित अन्य श्रेणियों में आता हो।
8. कोई बच्चा निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए कैसे आवेदन कर सकता है?
कोई बच्चा अपने माता-पिता/कानूनी अभिभावक के माध्यम से कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकता है।
9. क्या निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने या आवेदन पत्र जमा करने के लिए कोई शुल्क देना होगा?
नहीं, निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने या जमा करने के लिए कोई शुल्क नहीं है।
10. कानूनी सहायता के लिए आवेदन का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया क्या है?
जांच और मूल्यांकन समितियां कानूनी सेवा के लिए आवेदन का मूल्यांकन करेंगी और निर्णय लेंगी कि आवेदक नालसा (निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएं) विनियम 2010 के विनियम संख्या 7 के अनुसार कानूनी सेवा का हकदार है या नहीं।
11. कानूनी सेवाएं कब वापस ली जा सकती हैं?
- जब सहायता प्राप्त व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन हों।
- जहां सहायता प्राप्त व्यक्ति ने गलत बयानी या धोखाधड़ी से कानूनी सेवाएं प्राप्त की हों।
- जहां सहायता प्राप्त व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण/समिति या विधिक सेवा अधिवक्ता के साथ सहयोग नहीं करता है।
- जहां व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण/समिति द्वारा नियुक्त विधिक व्यवसायी के अलावा किसी अन्य विधिक व्यवसायी को नियुक्त करता है।
- सहायता प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, सिवाय सिविल कार्यवाही के मामले में जहां अधिकार या दायित्व कायम रहता है।
- जहां कानूनी सेवाओं के लिए आवेदन या संबंधित मामला कानून की प्रक्रिया (या) कानूनी सेवाओं का दुरुपयोग पाया जाता है।
12. कानूनी सहायता के लिए आवेदन स्वीकृत होने के बाद क्या प्रक्रिया है?
आवेदन स्वीकृत होने के बाद, आवेदक को वकील की नियुक्ति की सूचना दी जाती है। नियुक्त वकील को नियुक्ति पत्र भी जारी किया जाता है, जिसकी एक प्रति आवेदक को भी भेजी जाती है। इसके बाद, वकील जल्द से जल्द आवेदक से संपर्क करेगा। आवेदक भी इस बीच वकील से संपर्क कर सकता है।
13. यदि निःशुल्क कानूनी सेवाओं के लिए आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है तो क्या अपील की जा सकती है?
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम 2010 के विनियम 7(5) के अनुसार, विधिक सेवाओं के लिए आवेदन की जांच सदस्य-सचिव या सचिव द्वारा की जाएगी और यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन पर लिए गए निर्णय से व्यथित है, तो उसके पास विधिक सेवा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष के समक्ष अपील करने का विकल्प होगा और अपील के परिणामस्वरूप होने वाला निर्णय अंतिम होगा।
14. पैनल वकील कौन है?
“पैनल वकील” से तात्पर्य राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम 2010 के विनियम 8 के अंतर्गत चयनित वकील से है, जो योजना के अंतर्गत पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा प्रदान करता है।
15. रिटेनर वकील कौन है?
“रिटेनर वकील” का अर्थ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएँ) विनियम, 2010 के विनियम 8 के अंतर्गत चयनित रिटेनर वकील है। विधिक सेवा संस्थाएँ, पैनल वकीलों में से विधि व्यवसायियों की एक सूची तैयार करेंगी जिन्हें रिटेनर के रूप में नामित किया जाएगा जो फ्रंट ऑफिस में बैठेंगे और विधिक सेवा संस्थाओं में आने वाले वादियों को कानूनी सलाह देंगे। रिटेनर वकील अपना समय विशेष रूप से विधिक सहायता कार्य के लिए समर्पित करेंगे और संबंधित विधिक सेवा संस्थाओं में विधिक सहायता कार्य और फ्रंट ऑफिस का संचालन करने के लिए उपलब्ध रहेंगे।
16. कानूनी सहायता बचाव वकील कौन है?
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले के भीतर आपराधिक मामलों में कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता बचाव परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जाती है। वे कानूनी सहायता बचाव परामर्शदाता कार्यालय से जुड़े होते हैं और केवल कानूनी सहायता सेवाएँ प्रदान करने के लिए समर्पित होते हैं, अर्थात वे कोई भी निजी कानूनी मामला नहीं ले सकते। वे न तो सरकारी वकील या अधिवक्ता होते हैं और न ही लोक सेवक।
17. पैरा लीगल स्वयंसेवक कौन है?
कानून और अन्य उपलब्ध कल्याणकारी उपायों और विधानों का बुनियादी ज्ञान रखने वाले तथा अपने निकटतम पड़ोसियों की सहायता करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को संबंधित विधिक सेवा संस्थान द्वारा पैरा लीगल वालंटियर के रूप में चुना जाता है तथा विधिक सेवा नेटवर्क में सुधार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
18. पीएलवीएस को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया क्या है?
पैरा लीगल वालंटियर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्षों एवं सचिवों की देखरेख में आयोजित किया जाएगा।
प्रशिक्षण के छह सत्रों के पूरा होने के बाद, जिले में चिन्हित पीएलवी के एक बैच को प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पीएलवी की पंजीकृत संख्या और नामों की समेकित सूची राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।
सचिव डीएलएसए द्वारा तीन महीने में एक बार प्रशिक्षित पीएलवी के साथ बैचवार समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी और रिपोर्ट एक महीने के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।
1. लोक अदालत क्या है?
लोक अदालत भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान का एक मंच है। यह एक जन अदालत है जहाँ विवादों का निपटारा, लंबी अदालती कार्यवाही के बिना, सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जाता है।
2. लोक अदालत में किस प्रकार के मामले सुने जा सकते हैं?
लोक अदालतों में निम्नलिखित प्रकार के मामलों का निपटारा किया जा सकता है:
- सिविल प्रकृति का कोई भी मामला और
- समझौता योग्य आपराधिक मामले।
मुकदमेबाजी से पहले (अर्थात न्यायालय में मामला दायर होने से पहले) भी लोक अदालत में जाया जा सकता है। यदि उपरोक्त श्रेणी में आने वाला कोई मामला न्यायालय में लंबित है, तो संबंधित पक्ष न्यायालय से अनुरोध कर सकता है कि मामले को लोक अदालत में भेजा जाए।
हालाँकि, तलाक और आपराधिक मामलों से संबंधित मामले जो दंड प्रक्रिया संहिता के तहत गैर-समझौता योग्य हैं, उन्हें लोक अदालत में नहीं भेजा जा सकता है।
3. लोक अदालत में मामला भेजने के क्या लाभ हैं?
लोक अदालत में मामले के निपटारे के कई लाभ हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
- मामलों का निपटारा अत्यंत शीघ्रता से किया जाता है, जिससे पक्षकारों का बहुमूल्य समय बचता है।
- लोक अदालत में कोई शुल्क नहीं देना होता। पक्षकारों को किसी वकील की ज़रूरत नहीं होती। अगर मामला आपसी सहमति से निपट जाता है, तो पक्षकारों द्वारा चुकाई गई अदालती फीस भी वापस कर दी जाती है। इस तरह, पक्षकारों का पैसा बच जाता है।
- चूंकि लोक अदालत का निर्णय पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर तैयार किया जाता है, इसलिए वे अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे।
- लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय, दीवानी न्यायालय का आदेश माना जाता है। यह अंतिम होता है और विवाद के सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। इस निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। मुकदमेबाजी अंतिम होती है।
4. क्या लोक अदालत तलाक देने में सक्षम है?
नहीं, लोक अदालत तलाक नहीं दे सकती।
5. क्या लोक अदालत सिविल मुकदमों में निषेधाज्ञा (या) आपराधिक मामले में जमानत जैसी अंतरिम राहत दे सकती है?
नहीं। लोक अदालत ऐसी कोई राहत या अंतरिम निषेधाज्ञा या जमानत नहीं दे सकती।
6. लोक अदालतों की विशेष विशेषताएं क्या हैं?
-
- इसमें कोई न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क पहले ही चुका दिया गया है तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर वह वापस कर दिया जाएगा।
- विवाद के पक्षकार अपने वकील के माध्यम से सीधे न्यायाधीश से बातचीत कर सकते हैं, जो कि सामान्य न्यायालय में संभव नहीं है।
- लोक अदालत की मूल विशेषता अनौपचारिक, प्रक्रियात्मक और त्वरित न्याय है।
- लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है तथा इसे सिविल न्यायालय के निर्णय का दर्जा प्राप्त होता है तथा इस पर अपील नहीं की जा सकती।
- मूल निर्णय न्यायिक अभिलेख का हिस्सा होगा।
- यह निर्णय सिविल मामलों की तरह निष्पादन योग्य हो सकता है।
7. स्थायी लोक अदालत क्या है?
यह पीड़ित व्यक्ति और सार्वजनिक उपयोगिता सेवा प्रदाता के बीच विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक सस्ता मंच है।
8. सार्वजनिक उपयोगिता सेवा क्या है?
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-ए(बी) द्वारा परिभाषित सार्वजनिक उपयोगिता सेवा का अर्थ है-
- हवाई, सड़क या जल मार्ग से यात्रियों या माल के परिवहन के लिए परिवहन सेवा; या
- डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा; या
- किसी प्रतिष्ठान द्वारा जनता को बिजली, प्रकाश या पानी की आपूर्ति; या
- सार्वजनिक सफाई या स्वच्छता की प्रणाली; या
- अस्पताल या औषधालय में सेवा; या
- बीमा सेवा; या
- शिक्षा या शैक्षिक संस्थान;
- आवास और अचल संपत्ति सेवाएं और इसमें कोई भी सेवा शामिल है जिसे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, सार्वजनिक हित में, अधिसूचना द्वारा अधिनियम के अध्याय VI-ए के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर सकती है।
9. क्या सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालतें आपराधिक मामलों का निपटारा कर सकती हैं?
हां, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालतों को किसी अपराध से संबंधित मामलों के संबंध में क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जो किसी भी कानून के तहत समझौता योग्य हैं।
10. लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित किस प्रकार के विवादों का निर्णय लोक उपयोगिता सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालतें करेंगी?
सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालतें सभी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित सेवा में कमी, क्षति/मुआवजे के लिए दावे, धन की वसूली आदि से संबंधित विवादों का फैसला करेंगी।
11. जनोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालतों के समक्ष आवेदन कैसे दायर किया जा सकता है?
जनोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालतों में किसी भी कार्यदिवस पर सादे कागज़ पर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें सही और सटीक तथ्य और उस व्यक्ति/प्राधिकरण/जनोपयोगी सेवा प्रदाता का विवरण दिया गया हो, जिसके विरुद्ध राहत का दावा किया जा रहा है। हालाँकि, ऐसे आवेदन के साथ सहायक दस्तावेज़ और प्रतियाँ संलग्न होनी चाहिए जिन्हें विरोधी पक्ष को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
12. क्या सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत में सुनवाई के दौरान पक्षकारों का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है?
हाँ। पक्षकारों के बीच सुलह कार्यवाही के समय पक्षकारों का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना आवश्यक है, लेकिन स्थायी लोक अदालत द्वारा मामले का संज्ञान लेने के लिए आवेदन दाखिल करते समय उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।
13. क्या स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) द्वारा पारित निर्णय अंतिम है या अपील योग्य है?
स्थायी लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय, चाहे वह गुण-दोष के आधार पर हो या समझौता समझौते के आधार पर, अंतिम होगा तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-ई (1) के अनुसार सभी पक्षों और इसके तहत दावा करने वाले व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगा और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-ई (4) के अनुसार किसी भी मूल वाद, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।